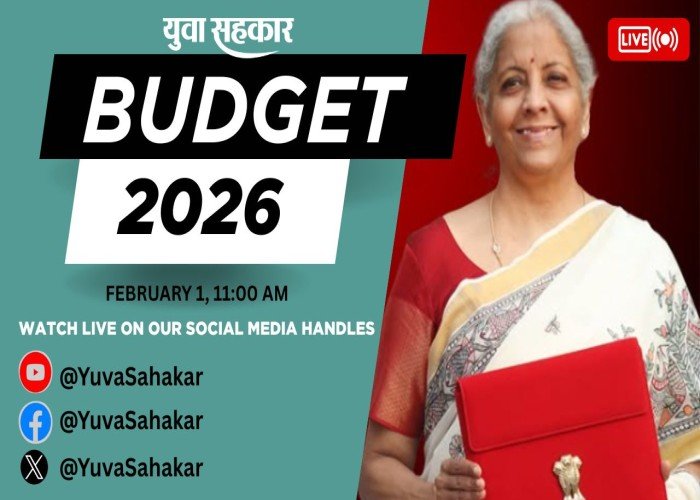रोजगार बढ़ाने को जरूरी है जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग का अधिक योगदान
जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 25 फीसदी करने का लक्ष्य अधूरा
मोबाइल निर्माण, तैयार स्टील और रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादों में मिली सफलता
सरकार ने वर्ष 2014 में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर को विकास का केंद्र मानते हुए वर्ष 2025 तक जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग की हिस्सेदारी को तब के 15-16 फीसद से बढ़ाकर 25 फीसद करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस उद्देश्य को पाने के लिए सरकार ने विशेष तौर पर मेक इन इंडिया अभियान भी चलाया। उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उपायों में प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव (पीएलआई) स्कीम भी विभिन्न उद्योग क्षेत्रों के लिए चलायी गईं। लेकिन इन सब उपायों का नतीजा सिफर ही रहा। आज भी देश की जीडीपी में उद्योगों की हिस्सेदारी 2014 के स्तर के आसपास ही घूम रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, यह करीब 17 फीसद है। जबकि कई अर्थशास्त्रियों की राय में यह इससे कम भी हो सकती है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक अजय श्रीवास्तव के मुताबिक यह हिस्सेदारी 13 फीसद तक नीचे आ चुकी है।
बीते एक दशक में ऐसा क्या हुआ कि सरकार की कोशिशों के बावजूद देश में मैन्यूफैक्चरिंग के योगदान में अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं हो सकी? हालांकि मेक इन इंडिया अभियान का एक दशक पूरा होने के बाद सरकार का दावा है कि कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला है। मसलन, इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर को देखें तो सरकार मानती है कि भारत में इस्तेमाल होने वाले 99 फीसद मोबाइल का निर्माण भारत में हो रहा है। इसके अतिरिक्त भारत अब तैयार स्टील उत्पादों का निर्यातक बन चुका है। यही नहीं रिन्यूबल एनर्जी के मामले में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसकी उत्पादन क्षमता में 400 गुणा इजाफा हुआ है।
सरकार ने मैन्यूफैक्चरिंग के विस्तार के लिए कई स्कीमों की घोषणा की। लेकिन पीएलआई जैसी स्कीम ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग खासतौर पर मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग को हैंडसेट असेंबली में केंद्रित कर दिया। देश में बनने वाले स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाले 90 फीसद कलपुर्जों का आज भी आयात किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जिस प्रकार अस्सी के दशक में आॅटो उद्योग को प्रोत्साहन देने के बाद कंपोनेंट इंडस्ट्री का विकास देश में बहुत तेजी से हुआ, वैसा मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग में नहीं हुआ। जबकि आज की तारीख में हम मोबाइल फोन निर्यात के मामले में भी अव्वल हैं। लगभग यही स्थिति रिन्यूबल एनर्जी सेक्टर में भी है। इसमें इस्तेमाल होने वाले पैनल व अन्य घरेलू उपकरण अत्यधिक लागत होने की वजह से आयात के मुकाबले महंगे पड़ते हैं। इसलिए बिजली उत्पादन में उतरने वाली अधिकांश कंपनियां आयातित उपकरणों का इस्तेमाल करती हैं। रक्षा क्षेत्र में उत्पादन को लेकर लचीला रुख अपनाने की वजह से इस क्षेत्र ने तेज विकास किया है।
यह सच है कि बीते एक दशक में अर्थव्यवस्था में बहुत से बदलाव आये हैं और इसका आकार भी बहुत तेजी से बढ़ा है। वित्त वर्ष 2014 में देश का जीडीपी 2010 अरब डॉलर का था। इसमें 314 अरब डॉलर के निर्यात भी शामिल थे। उस वक्त जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 15 फीसद थी। वित्त वर्ष 2024 में जीडीपी का आकार बढ़कर 3900 अरब डॉलर का हो गया है। निर्यात की हिस्सेदारी 437 अरब डॉलर की है। लेकिन मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान वहीं का वहीं है। श्रीवास्तव के एक आलेख के मुताबिक, वर्ष 2014 में भी आज की तरह मैन्यूफैक्चरिंग उत्पादों की देश के कारोबार में हिस्सेदारी 75 फीसद थी। लेकिन 2024 में जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग उत्पादों की तुलना में निर्यात की हिस्सेदारी 78.1 फीसदी से घटकर 64.6 फीसदी पर आ गई है। इसका मतलब यह हुआ कि कुल निर्यात में वृद्धि के बावजूद मैन्यूफैक्चरिंग उत्पादों के निर्यात में बीते एक दशक में कमी आई है।
मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर के लिए हमेशा से घरेलू और निर्यात बाजार उसकी वृद्धि की रफ्तार को तय करते आये हैं। वर्तमान में ये दोनों ही बाजार मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रहे हैं। सस्ते आयात की वजह से कई सेक्टर में घरेलू उत्पादों की मांग प्रभावित हो रही है। यही हाल निर्यात बाजार का भी है। अब सवाल यह उठता है कि वो कौन सी चुनौतियां हैं जिनकी वजह से मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पा रहा है? सबसे बड़ी दिक्कत उत्पादन की ऊंची लागत की है। चीन समेत कई दक्षिण एशियाई देश लागत के मामले में भारतीय उत्पादों को चुनौती दे रहे हैं। अगर हम औद्योगिक इस्तेमाल में आने वाली बिजली की लागत की बात करें तो चीन में प्रति किलोवाट इसकी लागत लगभग 0.06 से 0.08 डॉलर की आती है। जबकि भारत में यह 0.06 से 0.10 डॉलर की पड़ती है। यही नहीं उद्योगों को मिलने वाले कर्ज पर ब्याज की दरों में भी काफी अंतर है। भारत में जहां ब्याज की दरें 9-10 फीसद तक चली जाती हैं तो चीन में यह 4-5 फीसद ही रहती है। दक्षिण एशिया के कुछ देशों में तो सरकार निर्यात करने वाली मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयों को अन्य प्रकार के प्रोत्साहन भी देती है। यही वजह है कि थाईलैंड, वियतनाम जैसे कई देशों को बीते कुछ वर्षों में दुनिया के बड़े मैन्यूफैक्चरों ने विस्तार के लिए चुना।
श्रम कानून भी उद्योगों के विस्तार में बड़ी अड़चन बने हैं। सरकार ने इस दिशा में कदम उठाये हैं, लेकिन अभी भी इसमें कई तरह की कानूनी बाधाएं हैं जो कंपनियों में नई इकाइयां लगाने और पुरानी में क्षमता विस्तार के लिए हिचाकिचाहट पैदा करती है। भारत के मुकाबले चीन, वितयनाम और बांग्लादेश ने भारत के मुकाबले श्रम कानूनों को ज्यादा लचीला बनाया है। इसके अतिरिक्त नीति निरंतरता और दीर्घकालिक टैक्स नीति के अभाव ने भी मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर को प्रभावित किया है। यही वजह रही है कि आजादी के बाद मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में योगदान कभी तेज रफ्तार से नहीं बढ़ पाया। 1950 के दशक में यह अगर 8-9 फीसदी था तो 1980 के आसपास यह 14-16 फीसदी तक ही पहुंच पाया। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के वक्त यह माना गया था कि इससे अर्थव्यवस्था में मैन्यूफैक्चरिंग की भागीदारी तेजी से बढ़ेगी, किंतु ऐसा हो न सका। हालांकि 2000 के दशक में इसमें कुछ तेजी आई और यह लगभग 16-17 फीसदी तक जा पहुंचा। कोविड काल को छोड़ दिया जाए तो मैन्यूफैक्चरिंग का योगदान 13-17 फीसद के बीच ही घूम रहा है।
मैन्यूफैक्चरिंग की रफ्तार को सरकार के कुछ अन्य फैसलों ने भी प्रभावित किया है। खासतौर पर अति लघु, लघु और मझौले उद्योग इन फैसलों से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। एमएसएमई के नाम से जाना जाने वाला यह सेक्टर रोजगार मुहैया कराने के मामले में काफी अहम है। लेकिन ऊंची ब्याज दरों, कोलेटरल की शर्त और पहले नोटबंदी और फिर जीएसटी ने इस क्षेत्र की कमर ही तोड़ दी। रही सही कसर कोविड ने पूरी कर दी। उसके बाद से यह क्षेत्र उबर नहीं पाया है। निर्यात में भी इस क्षेत्र की हिस्सेदारी प्रभावित हुई है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों की मंदी और विदेशी उत्पादों की कम लागत ने इस क्षेत्र के निर्यातकों को प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया है।
कई सेक्टरों में आयात शुल्क में कमी और द्विपक्षीय व मुक्त बहुपक्षीय कारोबारी समझौतों की वजह से देश में आयातित सामान की उपलब्धता आसान हो रही है। खासतौर पर महंगे उत्पादों के मामले में यह ट्रेंड अधिक देखने को मिला है। इन आयातित उत्पादों की मांग देश में तेजी से बढ़ी है जिनकी वजह से घरेलू उत्पादों की मांग कम हो रही है। कॉस्मेटिक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान में यह ज्यादा अधिक स्पष्टता से दिख रहा है। इसके परिणाम स्वरूप घरेलू एफएमसीजी कंपनियों के कई उत्पादों को घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा में टिके रहना मुश्किल हो रहा है।
इस बात से किसी को इनकार नहीं होगा कि मैन्यूफैक्चरिंग और व्यापार (घरेलू व विदेश) दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। मैन्यूफैक्चरिंग की गुणवत्ता ही निर्यात को बढ़ाएगी और निर्यात बाजार में पैठ ही मैन्यूफैक्चरिंग को विस्तार का अवसर देगी। बीते एक दशक के अनुभव ने यह साबित किया है कि केवल प्रोत्साहन ही जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग के योगदान को बढ़ाने के लिए काफी नहीं हैं। उद्योगों के लिए ऐसी टिकाऊ टैक्स और प्रोत्साहन नीति का समन्वय करना होगा जो न केवल लागत कम करे बल्कि आयातित उत्पादों के साथ घरेलू उत्पादों को भी प्रतिस्पर्धी बनाने में मददगार हो। सरकार ने 2025 में जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग के 25 फीसदी के योगदान के लक्ष्य को अब 2030 तक के लिए आगे बढ़ाया है। इस लक्ष्य को पाना है तो अगले छह वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होंगे।
देश में बनने वाले स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाले 90 फीसद कलपुर्जों का आज भी आयात किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जिस प्रकार अस्सी के दशक में ऑटो उद्योग को प्रोत्साहन देने के बाद कंपोनेंट इंडस्ट्री का विकास देश में बहुत तेजी से हुआ, वैसा मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग में नहीं हुआ। बीते एक दशक में अर्थव्यवस्था का आकार भी बहुत तेजी से बढ़ा है। 2014 में देश का जीडीपी 2010 अरब डॉलर का था। उस वक्त जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 15 फीसद थी। 2024 में जीडीपी का आकार बढ़कर 3900 अरब डॉलर का हो गया है लेकिन मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान वहीं का वहीं है।